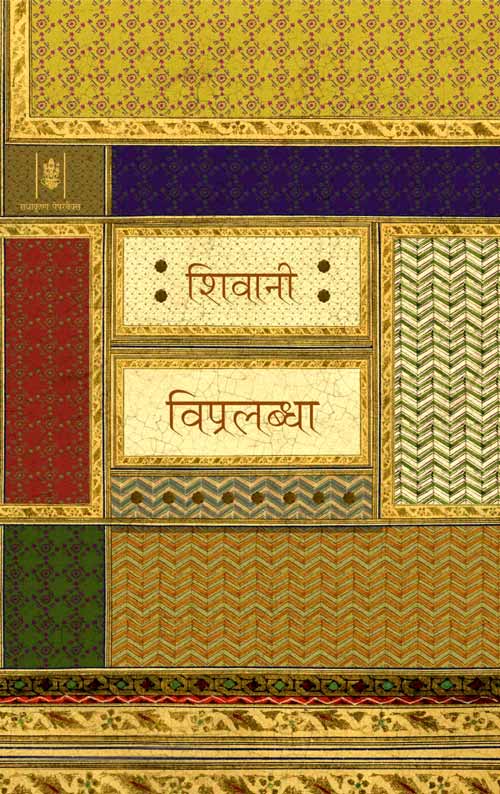

Vipralabdha

Vipralabdha
₹125.00 ₹105.00
₹125.00 ₹105.00
Author: Shivani
Pages: 134
Year: 2007
Binding: Paperback
ISBN: 9788183611138
Language: Hindi
Publisher: Radhakrishna Prakashan
- Description
- Additional information
- Reviews (0)
Description
विप्रलब्धा
दो स्मृति-चिह्न
बिन्दु की आँखों में नींद नहीं थी। उसने बड़ी ललक से, गहरी नींद में डूबे अपने पति को निहारा। नींद में उसका चेहरा किसी निर्दोष भोले बालक का-सा लग रहा था। बालों का एक फुग्गा हवा में उड़-उड़कर चेहरे पर झुका आ रहा था। धीरे-से बिन्दु ने गुच्छे को सहलाकर पीछे किया तो देवेश जग गया।
‘‘अमाँ, सोने दो, यार !’’ कह वह फिर से करवट लेकर सो गया। बिन्दु को हँसी आ गई। कैसी नींद है बाप रे बाप ! उसकी तो आँख ही नहीं लगी थी। लगती भी कैसे ?
एक लम्बी साँस खींचकर उसने दीवार की ओर मुँह फेर लिया। कितनी बदल गई थी इन्दु ! बात-बात पर रोनेवाली दुबली-पतली इन्दु को वह आज कहीं भीड़-भाड़ में देखती तो शायद पहचान भी न पाती। कल ही तो उसकी चिट्ठी आई थी। वह तो अच्छा था कि दिन-रात बाहर घूमने वाले फक्कड़ युगल दम्पति उस दिन घर पर ही थे। कहीं इधर-उधर गए होते तो शायद इन्दु की ट्रेन निकल भी जाती। आठ वर्षों से बिछुड़ी बहन को क्या वह फिर देख पाती ? उसकी आँखें बार-बार भर आ रही थीं। बाबूजी सगी माँ और पाँचों बहनों ने तो उसे दूध की मक्खी-सी समझ कर फेंक दिया था। वह मरी है या जिन्दा, क्या कभी किसी ने खोज-खबर भी ली थी ? बड़ी दी के लड़के का विवाह हुआ, दूर-दूर के आत्मीय स्वजनों को भी साड़ियाँ बाँटी गईं, पर सगी छोटी बहन को दो अक्षर कोरे निमंत्रण के भी नहीं भेज सकीं ! मँझली दीदी तो उसे बुला सकती थीं। उनकी तो दोनों देवरानिया विजातीय थीं—एक पंजाबी, दूसरी बंगाली।
पर उन्होंने पुत्र के जनेऊ का निमंत्रण नहीं भेजा। तीसरी बहन तो पति के साथ विलायत भी घूम आई, पर आठ वर्ष पहले अपनी सहेली के भाई से अन्तर्जातीय प्रेम-विवाह करनेवाली बिन्दु को क्षमा नहीं कर सकी। मायके ने उस दक्ष-कन्या की स्मृति को लेकर कोलतार की झाड़ू ही फेरकर रख दी थी ! बरेवाली मामी ही उसे सारी खबरें देती रहतीं। मायके-रिश्ते में एक स्नेही मामी का ही क्षीण सूत उसके आँचल से बँधा रह गया था। मामी को भी जीभ का कैन्सर हो गया था और वह तागा कभी टूट सकता था। फिर अचानक इन्दु की वह प्यारी-सी चिट्ठी आ गई थी। उसकी सबसे छोटी और सबसे प्यारी बहन। उसका विवाह हो गया है, यह सूचना मामी ने दी तो वह पति से छिपकर एकान्त में खूब रोई थी। कितनी सुन्दर थी इन्दु और वह एक सड़े-से क्लर्क को ब्याह दी गई ! ‘इन्दु के विवाह में तुझे बुलाने को मैंने तेरी माँ को पटा लिया था, पर तेरे दुर्वासा से बाबूजी ने तो मुझे चीरकर रख दिया !’ मामी ने लिखा था—‘बोले, ख़बरदार, उस कुलबोरिनी को बुलाया ! हमारे लिए तो वह मर-खप गई ! ब्राह्मण की बेटी बनिए की बहू बनने गई तो कहो, वहीं बनी रहे।’’
यह ठीक था कि उसने पारम्परिक श्रृंखला को चूर कर देवेश जालान से विवाह किया था, पर क्या वह सुखी नहीं थी ? श्वसुर का वैभव, पति की ऊँची नौकरी, नौकर-चाकर, मोटर, फ्रिज, सब उसके करतल पर धरे थे। ऐसा सुख क्या उसे अपने समाज में मिलता ? पर फिर भी एक अदृश्य काँटे की चुभन रह-रहकर क्यों सालती रहती थी ? क्यों वह काँटे का सिरा खींचकर नहीं निकाल फेंकती ? उस कांटे को अब विधाता भी नहीं निकाल सकता। वह काँटा है विषैला गोखुर कंटक। अपने समाज, अपनी संस्कृति की स्मृति का काँटा। इन्दु की शादी में तीनों मामियाँ आई होंगी। छुहारे, किशमिश, डली पहाड़ी सोंठ के कठौते में भरी उसी आले पर धरी छलकती होगी, जहाँ मँझली दी के विवाह की सोंठ धरी गई थी और जहाँ से उसने इन्दजुली को चार हाथ-पैरटेक, घोड़ा बना, सावारी कर, काँसे का कटोरा भर सोंठ चुराई थी।
फिर दोनों बहने पिछवाड़े के दालान में छिप गई थीं। और कटोरा दो चटोरी जिह्वाओं ने मलकर पल-भर में चमका दिया था। कभी-कभी पड़ोस की हिरुली इसाइन अम्मा की आँखें बचा दोनों बहनों को अपनी लेगहार्न मुर्गी का बड़ा-सा अंडा दे, तसला भर आटा माँग ले जाती। दोनों फिर हिरुली के यहाँ एक जंग लगे सार्डिन की टीन में अंडा उबाल तिमिल के वृक्ष की घनी छाया में दुबक जातीं। उसी वृक्ष की उदार छाया में ऐसे अनेक अखाद्य म्लेच्छ सामाग्रियों के बँटवारे होते रहते थे। बहन की निगरानी में, सार्डिन की टीन की तीखी धार में उबले अण्डे को समान भाग में विभक्त कर, उसके नमक लेकर आने तक न खाने की विद्या-कसम दिला बिन्दु लौटती तो दोनों कटे भागों की पिलौंदी सन्दिग्ध अवस्था में नुची मिलती। स्पष्ट रहता कि उसकी अनुपस्थिति में छोटी बहन की लोलुप जिह्वा धैर्य की लक्ष्मण-रेखा लाँघ चुकी है।
‘‘पिलौंदी खाकर तूने फिर हाथ से बैठाई ! इन्दुली, खा विद्या-कसम !’’ बिन्दु कहती।
‘‘विद्या-कसम !’’ इन्दु कसम खाने को अपने रसीले अधर-द्वय फैलाती और नन्हीं जीभ की नोक में लगी जर्दी में बिन्दु को त्रैलोक्यदर्शन हो जाते। फिर तो खूब झोंटा पकड़ा-पकड़ी होती।
ऐसी ही झपट जलेबी आने पर भी होती रहती। बाबूजी कभी-कभी कचहरी से जलेबी का दोना ले आते, आले पर धरकर हाथ-मुँह धोने जाते तो इन्दुली चुपचाप आकर, किसी वैम्पायर की भाँति, जलेबियों का रस-समुद्र पलभर में सोख बड़ी बहन के लिए जलेबियों का अस्थिपंजर-मात्र छोड़ देती पर बिन्दु बहन की भाँति नासमझ और लालची नहीं थी। अंग्रेजीभक्त स्कूल में पढ़ी थी, इसी से उसकी चाल-ढाल, आचार-व्यवहार में एक सुघड़ सलीका था। उसके मामा अंग्रेजी स्कूल में क्लर्क थे और उन्हीं की कृपा से उसने बिना फीस दिए ही सीनियर कैम्ब्रिज पास कर लिया था। वह छुट्टियों में घर आती तो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलनेवाली अपनी बिटिया को देखकर बाबूजी खिल उठते—‘‘आ गई हमारी अंग्रेज़ बिटिया ! अब अपनी इस गँवार बहन को भी अंग्रेजी बोलना सिखा दे। इसे तो पास-पड़ोस के कच्चे सेब-खुबानी चुराने से ही फुरसत नहीं मिलती !’’
इन्दुली बिदक जाती—‘‘हमें नहीं सीखनी अंग्रेज़ी ! ज़रा सप्तमी में ‘लता’ और ‘राम’ के रूप बता दे नान दी तो हम भी जानें !’’ वह बड़े गर्व से हिल-हिलकर लता के रूप याद करने लगती।
संक्रान्ति को अम्मा गुड़ डालकर आटे के गुलगुले, ढाल-तलवार और फुलौ बनाकर घी में तलती। घी में पकते मीठे पकवान की खुशबू पूरे चौके में फैल जाती। फिर दोनों बहने बड़े यत्न से उन पकवानों को गूँथ माला बनातीं अनुपस्थित बहनों के नाम की—एक बड़ी दी की, दो उनके बच्चों की, फिर मंझली दी की, उनके बच्चों की, मँझली दी और उनकी पुत्री की, अन्त में स्वयं अपनी। इन्दुली फिर बेईमानी से सबसे बड़ी तलवार, गुजिया और संतरा, सब अपनी माला में गूँथ लेती। सुबह उठकर दोनों छत पर चढ़ कर एक-एक पकवान का टुकड़ा कौवे को दिखा-दिखा बुलातीं :
ले कौआ फुलौ,
मेंकें दियै भल-भल धुलौ।
(अरे कौवे, ले फुलौ और उसके बदले मुझे बढ़िया-सा दूल्हा ला दे।)
कैसा अजीब पहाड़ी त्यौहार था वह, जब झुंड के झुंड लाल-लाल गालों वाली, स्वस्थ सुन्दर, पहाड़ी लड़कियाँ फुलौ के पकवान शून्य आकाश में बिखेरतीं, भविष्य के सजीले दूल्हे की कामना करतीं ! युग-युगान्तर से कुमाऊँ का आकाश प्रत्येक उत्तरायण को ऐसे ही मधुर कलकंठ के काक-आह्वान से मधुमय होता रहा है और आज भी होता होगा। पर कहाँ है अब वह आकाश ! उस निर्मल आकाश में उड़ती हंस-बलाका की पंक्ति से वह उड़कर दूर छिटक गई है। अब तो वह सोने के पिंजरे में बंद राजा की मैना है। उसके श्वसुर कैनेडा में टिम्बर के व्यापारी हैं। दोनों देवरों ने विदेशी युवतियों से विवाह कर लिया था। वह पति के साथ विदेश जाती और समुद्र-तट पर इन्धनुषी छाते की छाया में दो-दो गिरह की कंचुकी और बित्ते-भर की रंगीन बिकनी में आलू के पापड़-सी सूखती औंधी लेटी सास और देवरानियों को देखती तो सिहर उठती।
पास के ही कैनवस की कुरसी पर मुँह में चुरट लगाए श्वसुर बैठे रहते। उनका बचकाना सूप-सा टोप, लाल-पीली धारीदार कौपीन और लाल नंगी पीठ देखकर कोई नहीं कह सकता कि वह भारतीय हैं। वर्षों से विदेश के प्रवास ने उनका रंग-रूप भी विदेशी साँचे में ढाल दिया था। देवेश तो समुद्र को देखते ही कपड़े समुद्र-तट पर पटक, बच्चे-सा किलकता कूद पड़ता, पर लाख समझाने पर भी, सास श्वसुर की उपस्थिति में बिन्दु श्वसुर-कुल की सूर्य-स्नान की परम्परा नहीं निभा पाती। मूर्खा-सी खड़ी ही रहती। उसकी सास की उस पर विशेष कृपा थी उन्हें विदेश में रहते-रहते बीस वर्ष हो गए थे, इसी से भारत से ब्याह कर लाई गई इस सकुचाती सुन्दरी पुत्र-वधू के सलज्ज आचरण पर वह पहली बार मुग्ध हो गईं। स्वयं उनकी पुत्री, जो भारत में शिक्षिता होने पर भारतीयता नहीं ग्रहण कर सकी, उनके लिए अब बहुत बड़ा सिरदर्द बन गई थी।
वह भारत के ही प्रसिद्ध किसी होटल में रिसेप्शनिस्ट थी, उसी की मैत्री बिन्दु को इस घर में लाई थी। सास की लाड़ली बहू थी बिन्दु, पर वह बेचारी तो अब एक दूसरे ही प्रकार के लाड़ के लिए तरसने लगी थी। मँझली दी की सास का-सा लाड़—क्षणे रुष्टा, क्षणे तुष्टा। एक दिन मायके आई तीनों बच्चों की माँ मँझली दी को नैनीताल के फ्लैट में बहनों के साथ आलू की टिकिया खाते देख लिया, तो वहीं पर चीरकर रख दिया था—‘‘बेहया कैसी सिर उघाड़ रंडियों सी घूम रही है ! क्यों, इसी चटोरेपन के लिए मायके आती है तू, बहू !’’ मँझली दी की हाथ की टिकिया नीचे गिर पड़ी थी और थर-थर काँपने लगी थीं बेचारी। पर उसी सास ने सात तोले की पलचड़ भी तो गढ़वा दी थी मँझली दी को। स्कूल के जलसे में उसी के हार से सजी इन्दुली को चाँदी का-बड़ा-सा कप मिला था। बड़ी दी के सफेद रेशमी साड़ी पहन इन्दु सरस्वती बन गई थी। आज वही इन्दु आ रही थी। टोकरी भरकर उसने स्टेशन के लिए तीन ही बजे तैयारी कर ली थी।
एक दर्जन भर उबले अंडे थे। जी भरकर ज़र्दी खाएगी, इन्दुली। गर्म-गर्म जलेबियों का अमबार था। बस, एक ही चीज़ नहीं मिल पायी थी और उस चीज़ पर तो इन्दुली ही नहीं, भारत के प्रत्येक प्रान्त की इन्दुली मर मिटती हैं—हरी-हरी अमिया। एक तो पहाड़ पर अमिया सदा ही मोती के मोल बिकती थी। कभी छठे-छमाहे छटी नामकर्म में दोनों बहनों को दुवन्नी-चवन्नी का आर्थिक लाभ होता तो भागती सब्जी मार्केट। कभी-कभी तो दोनों सम्मिलित धनराशि से एक ही अमिया जुटा पाती, फिर उसे छीलकर नमक चुपड़, बारी-बारी से चाटने की क्रिया में भी दुष्टा इन्दुली की जिह्वा में न जाने कैसे बत्तीसी उग आती। इन्दुली बड़ी कुशलता से बत्तीसी अंकित अमिया का अंश छिपाकर बहन को थमाती पर बिन्दु दन्तक्षत देखकर हँस देती। आज अमिया मिलती, तो वह टोकरी भरकर ले आती। कोई बात नहीं, साथ में इन्दुली का नन्हा पुत्र भी आ रहा था, उसके लिए कई मिल्क-बार चॉकलेट रखना भी नहीं भूली था बिन्दु।
स्वयं उसके कोई संतान नहीं थी, इसी से अनुभवहीना बिन्दु यह नहीं जानती थी कि दस माह का भगिनी-पुत्र एक साथ उतनी चॉकलेट नहीं पचा सकता।
पति को लेकर वह स्टेशन पहुँची, तो गाड़ी आ चुकी थी। वातानुकूलित डिब्बों में सफर करने का अभ्यस्त उसका अनाड़ी पति, उसकी बहन को उन्हीं डिब्बों में ढूँढ़ रहा था, पर वह तेजी से आगे बढ़ गई। वह जानती थी कि एक क्लर्क को ब्याही गई उसकी बहन उसे किस डिब्बे में मिलेगी। हाथ में भारी टोकरी लटकाए वह इधर-उधर देखती जा रही थी। कभी बक्सों का अंबार बनाए किसी कुली से टकरा जाती, तो वह झुँझला उठती। इस प्रकार के रेलम-पेलम में घुसपैठ का उसे अभ्यास नहीं था। कभी पति-पत्नी किसी यात्रा पर जाते, दो-तीन नौकर, स्टेनो उनका रिजर्वेशन कर आते थे। वह बढ़ती जा रही थी।
‘‘ओ नान दी…नान दी री, यहाँ हूँ मैं !’’
Additional information
| Authors | |
|---|---|
| Binding | Paperback |
| ISBN | |
| Language | Hindi |
| Pages | |
| Publishing Year | 2007 |
| Pulisher |





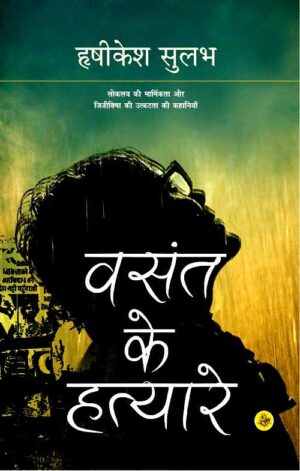
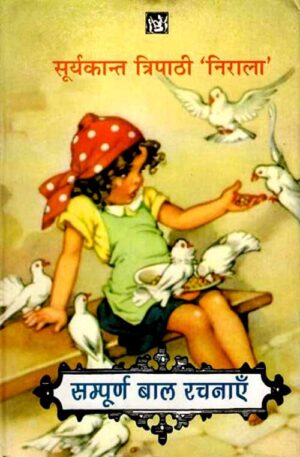
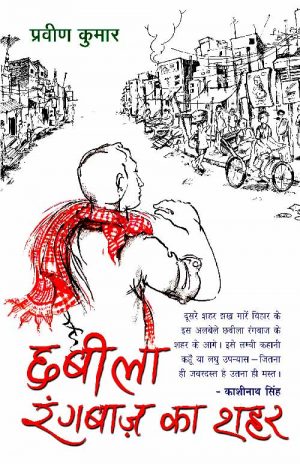
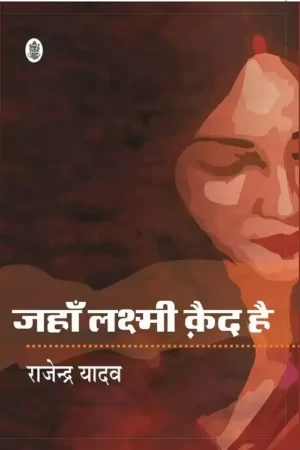
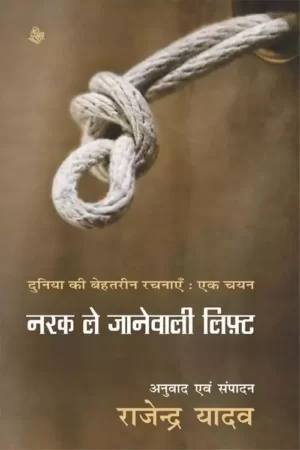


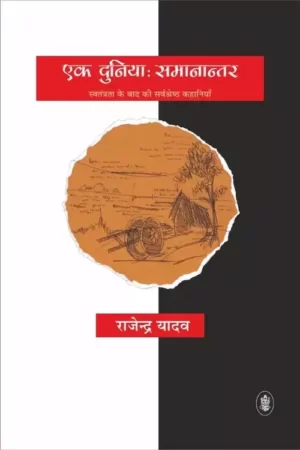
Reviews
There are no reviews yet.